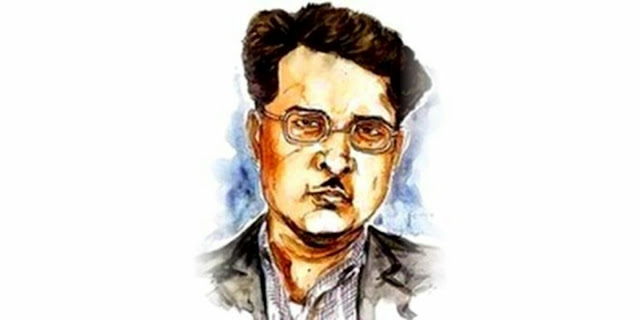केवल 52 वर्षों की आयु पाने वाले नेपाली हिंदी के उन गिने चुने कवियों में हैं जिनका जनता से गहरा सरोकार रहा।
11 अगस्त, 1911 को बिहार मे शहर बेतिया के कालीबाग दरबार के नेपाली महल में जन्में शायद इसीलिए गोपाल बहादुर सिंह ने कविताऍ लिखनी शुरु कीं तो नेपाली संज्ञा को अपने नाम के साथ जोड़ा। मैट्रिक तक की तालीम भी हासिल न कर पाने वाले नेपाली ने बेतिया राज के समृद्ध पुस्तकालय में बैठकर ही यदा कदा साहित्या का अध्य यन-अवगाहन किया। क्यूंकि अपने सैनिक पिता के साथ विभिन्नह जगहों–यहाँ तक कि छावनियों तक में रहने के कारण उनका जीवन प्राय: बिखरा हुआ ही रहा।
शमशेर जिसे टूटी हुई बिखरी हुई की संज्ञा देते हैं वह दरअसल नेपाली के जीवन से ज्याखदा जुड़ती है। पर हाँ इस बिखराव के बीच जीवन और संसार को नए ढंग से देखने-परखने का अवसर उन्हें अवश्य मिला। वे इतने होनहार थे कि उनकी रचनाऍं तब की श्रेष्ठ पत्रिकाओं, युवक, विशाल भारत, हंस, सरस्वती, कर्मवीर, और प्रताप में प्रकाशित होती थीं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनकी पहली कविता अपनी पत्रिका बालक में छापी थी। अपने समय के बड़े लेखकों से उनकी मैत्री रही। बेतिया उन दिनों साहित्य के साथ साथ संगीत का भी केंद्र हुआ करता था।
ध्रुपद के बोलों से कदाचित उन्हों ने अपनी कविता को छंदों मे ढालने की प्रेरणा ली होगी।
बेतिया के साहित्यिक माहौल की ही यह असर है कि मात्र 22 साल की उम्र मे उनका पहला कविता संग्रह उमंग छपा, दो साल बाद दूसरा संग्रह पंछी आया, फिर रागिनी, नीलिमा, पंचमी और नवीन शीर्षक संग्रह आए। हिमालय ने पुकारा उनके राष्ट्रीय गीतों का संग्रह है। उनके कविता संग्रहों की भूमिकाएँ उस दौर के दिग्गज कवियों ने लिखीं। पंछी की भूमिका निराला ने लिखी। उमंग की भूमिका पंत ने, नीलिमा की भूमिका योगी के संपादक व्रजशंकर वर्मा ने तो हिमालय ने पुकारा की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर ने। चीनी आक्रमण के दौर में उनकी अनेक कविताएँ तत्कालीन लोकप्रिय व्याावसायिक पत्रिका धर्मयुग में प्रकाशित हुईं। नेपाली ने पत्रकारिता में भी जोर आजमाइश की। शुरुआती दौर में प्रभात और दि मुरली पत्रिकाएँ निकालीं तो आगे चल कर निराला जी के साथ सुधा पत्रिका से भी जुड़े। रतलाम टाइम्स, पुण्यतभूमि और योगी पत्रिकाओं से भी उनका जुड़ाव रहा। अपने लेखकीय गुणों के कारण वे कुछ दिनों बेतिया राज के प्रेस प्रबंधक भी रहे। लोग कहते हैं, उनके गीतों की पदावली जितनी मधुर होती थी, उनका कंठ उससे भी मधुर और ओजस्विता का पर्याय था।
विस्मृति का धुँधलका और नेपाली
बचपन में पाठ्यचर्या के दौरान पढ़े हुए जिन कुछ गीतों का याद आज भी ताजा है उनमें यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल और तन का दिया प्राण की बाती दीपक जलता रहा रात भर जैसे गीत हैं। बड़े होने पर पता चला, इस गीत के रचयिता वही हैं जिन्हों ने मेरा धन है स्वारधीन कलम लिखा है। आज का युग ऐसा है कि बड़े से बड़ा कवि भी विस्मृंति के धुँधलके में ओझल हो सकता है। नेपाली जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे जब तक जीवित थे, यानी 1963 तक— तब तक उनके नाम और गीतों की धूम थी। वे मंच लूट लेने वाले कवियों में थे। पर पार्थिव सत्तान के ओझल होते ही याददाश्तों से गुम-से होते गए। वे विस्मृति के इसी धुँधलके में रहे आए होते यदि शताब्दी वर्ष में उन्हें याद न किया जाता। यहाँ तक कि उनकी रचनाएँ भी अभी तक लगभग अनुपलब्ध ही थीं। उनके रहते भी किसी बड़े प्रकाशक के यहाँ से उनकी कृति न छप सकी। कदाचित ऐसा होता तो उनकी कीर्ति की पताका फहराने वाली कृतियाँ हमारे बीच उपलब्ध रहतीं। शायद प्रकाशकों द्वारा उस दौर के साहित्यि क प्रतिमानों की कसौटी पर नेपाली जी कमतर ठहरते रहे हों, प्रकाशकीय उदासीनता की एक वजह यह भी हो सकती है। यही नहीं गोपाल सिंह नेपाली का नाम न केवल हिंदी की जगत से, बल्कि बालीवुड की दुनिया से भी गहरे से जुड़ा है। उनके सैकड़ों गीत जो फिल्मोंह के लिए लिखे और गाए गए, आज न केवल अनुपलब्ध हैं, बल्कि उनकी मुकम्मिल सूची तक हमारे पास नहीं है। जबकि नेपाली ने अपने गीतों को उस सिनेमाई आभा में नहीं रचा, जिस पर केवल फिल्मी होने का ठप्पा लगा कर उसे नजरंदाज किया जा सके। बल्कि फिल्मों के माध्यमम से उन्होंने जाना कि लोकप्रियता हासिल करनी है तो जनता की भाषा समझनी होगी और उसी तेवर में लिखना भी होगा। यह अचरज नहीं कि नेपाली के जेहन में रामधारी सिंह दिनकर की ‘समर शेष है’ कविता की ये पंक्तियाँ रही हों कि : ‘समर शेष है, नही पाप का भागी केवध ब्यावध / जो तटस्थ् हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध।‘ हिमालय ने पुकारा के साथ उनकी कविता में एक खास तरह की नैतिक आक्रामकता आई। एक और वजह यह भी हो सकती है कि दिनकर के दुर्ग में बिना ओज और वीर रस को हथियार बनाये लोकप्रियता की पायदान पर पहुँचना असंभव है। लिहाजा नेपाली की कविता में हिमालय ने पुकारा एक बड़े मोड़ का परिचायक बनी। चीन के आक्रमण ने उन्हें वह भावभूमि दे दी जिस पर खड़े होकर वे जनता की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दे सकते थे।
अलग राह: अलग छटा
कहना न होगा कि जिस दौर की साहित्यिक अंतर्धारा में प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत का वर्चस्वच रहा हो, छायावादोत्तार दौर के कवियों में बच्चन और दिनकर लोकप्रियता के शिखर पर रहे हों, उनके बीच जनसमूह की कसौटी पर लोकप्रिय कवि बनना आसान न था। किन्तु नेपाली सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे। उन्हों ने लोकमानस में उतरने के लिए अपनी राह अलग तैयार की। न तो उन्होंने छायावादी भाव-भूमि को अपनी रचनाओं में प्रश्रय दिया, न ही वे रहस्यवादी कल्पशनाओं का संजाल में घिरे, बल्कि निराला से संपर्क के कारण उनके गीतों के रचाव में कहीं न कहीं एक खास तरह की निराली छटा देखने को अवश्यक मिलती है। गीतों में उनकी शख्सियत खुल कर बोलती थी। पर जैसा कह आया हूँ, अपनी रचनाओं में वे सर्वथा अलग दिखते हैं तो अलग दिखते ही नहीं, अपने समवर्ती और अनुवर्ती कवियों-गीतकारों पर अपनी अलग छाप भी छोड़ते हैं। वे फिल्मी दुनिया से भी जुड़े तो अपनी शर्तों पर। उनके अनेक साहित्यिक गीत फिल्मों में ज्यों के त्यों लिए गए। थोड़ी सी अवधि में उन्होंने लगभग 300 गीत फिल्मों के लिए लिखे और ऐसी अपार लोकप्रियता हासिल की जो विरल लेखकों को मिलती है। फिल्मों में लिखे उनके गीतों में कुछ गीतों के बोल हैं– ओ दुपट्टा रंग दे मेरा रंगरेज, कहॉं तेरी मंजिल कहॉं है ठिकाना, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूँ, दूर पपीहा बोला रात आधी रह गयी, न जाने कैसी बुरी घड़ी दुल्हीन बनी एक अभागन, बहारें आऍंगी होठों पे फूल खिलेंगे, मेरी चुनरी उड़ाए लियो जाए, यहाँ रात किसी की रोते कटे या चैन से सोते सोते कटे और शमा से कोई कह दे । यहाँ भी देखें तो गीत भले ही फिल्मों के लिए हों, उसमें भी उनका अपना एजेंडा बोलता था। धार्मिक गीत लिखने में उनका कोई सानी न था। ‘दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अँखियाँ प्यासी रे’ जैसा भक्तिपूर्ण गीत लिखने वाले नेपाली के गीतों की अपनी प्रवाहमयता है। गीत का मुखड़ा जेहन में आते ही भाषा और भाव जैसे उनकी कल्पपना का स्वत: ही अनुसरण करते हैं। बालीवुड जाकर उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनियों हिमालय फिल्मस और नेपाली पिक्चर्स की स्थापना भी की तथा तीन फिल्में—नज़राना, सनसनी और खुशबू भी खुद बनायीं जिनमें उस दौर के जाने माने अभिनेताओं ने अभिनय किया। पर बाक्स आफिस पर इन फिल्मों के न चलने के कारण आर्थिक घाटा उठाना पड़ा। फलत:, बालीवुड की दुनिया उन्हें बाँध कर न रख सकी, वे एक कवि के रूप में अपनी जवाबदेही से विमुख न रह सके और आखिर में जनता-जनार्दन और राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने के लिए काव्य मंचों को समर्पित हो गए।
नेपाली के गीतों का अपना जादू रहा है। वे पाठ और पाठ्यबल दोनों के धनी थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं को लक्षित करते हुए निराला ने उनके काव्यक में शक्ति्, प्रवाह, सौंदर्यबोध और चारुता की सराहना की तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी कविता के भावों में कल्पना की आकाशव्यापी उड़ान दीख पड़ती थी। वीरेन्द्रं मिश्र को उनकी स्ववर लहरी में नदी का सा प्रवाह दीखता था। नरेन्द्र शर्मा को उनकी व्यंजना भाती थी तो नेपाली के निधन पर बच्चन का कहना था कि नेपाली के न रहने से माँ भारती की वीणा का एक तार टूट गया है। दिनकर ने नेपाली को रससिद्ध कवि और जनता का हृदयहार माना था। दिनकर से उन्होंने कहा था, ‘आई एम वन मैन आर्मी आफ इंडिया।‘ और यह भी कि ‘मैं जानता हूँ कि मुझको कोई पद्मश्री या पद्मभूषण की उपाधि नहीं प्रदान करेगा, किन्तु जब पीकिंग रेडियो मेरा नाम लेकर मुझे गालियाँ देता है तो मुझको लगता है कि शायद मुझको उन उपाधियों से कहीं ज्यादा मिल रहा है।‘ कहने को दिनकर अपने समय के सर्वाधिक ओजस्वी कवि थे। उनकी हुंकार ने देश के स्वाभिमान को ललकारा था। पर वे सत्ता के नजदीक रहे। पंडित नेहरू के प्रिय थे। शुद्ध कविता की खोज से लेकर संस्कृति के चार अध्यातय तक उनकी अप्रतिहत बौद्धिक तेजस्विपता के आगे नेपाली को कौन पूछता । किन्तु नेपाली सत्ता के मुखापेक्षी नही रहे। कविता में अपना नायकत्व उन्होंने स्वयं प्रतिष्ठिपत किया। यद्यपि कवि सम्मेलनी और फिल्मीं का ठप्पा लगाकर साहित्य में उनके लिए बैरियर खड़े किये गए जैसा आज भी सार्वजनिक जीवन के कवियों के साथ होता है, किन्तु नेपाली को अपने कृतित्वि पर भरोसा था और जनता के मध्य अपनी भूमिका का अहसास। खेतों की हरी-भरी चादर और गंगा किनारे उनकी तबीयत लगती थी। उनकी आँखों की करुणा में गंगा-जमुना का वास था।
फिल्म जगत और नेपाली
गोपाल सिंह नेपाली का कवि-कद बेशक बड़ा न हो पर उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कवि सम्मेलनों में ‘वन्स मोर वन्स मोर’ का शोर तब तक नहीं थमता था, जब तक नेपाली पुन: जनता के सम्मुख आ न खड़े होते। मुम्बई में कवि सम्मेलनों में उन्हें सुनकर ही फिल्मिस्तान ने उनसे फिल्मों में गीत लिखने का अनुबंध किया था। उन दिनों नेपाली के हालात भी कुछ ऐसे थे कि जीवन यापन के लिए एक नियमित आमदनी जरूरी थी। लिहाजा साहित्यिक गीत लिखने वाले इस कवि को फिल्मी दुनिया की व्यवसायिकताओं से समझौता करना पड़ा। किन्तु नेपाली यहाँ भी सफल रहे। यदि हम फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने गए कवियों पर निगाह डालें तो आजादी के पहले कभी भवानीप्रसाद मिश्र ने भी किसी फिल्म निर्माता को अपने कुछ गीत दिए थे, किन्तु कुछ अखबारों में प्रतिकूल टिप्पणियों के चलते भवानी भाई ने फिल्मों से तोबा कर लिया और यह मशहूर गीत लिखा, ‘जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ !’ जो बाद में उनकी कुछ बेहतरीन कविताओं में मानी गयी। उसके बाद इस दुनिया में प्रदीप आए। देशभक्ति गीत लिखने में प्रदीप जी अपनी मिसाल खुद थे। सन बयालिस में उनके लिखे गीत ‘आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है/दूर हटो-दूर हटो-ऐ दुनिया वालों, हिन्दुस्तान हमारा है’ ने यह हालात पैदा कर दिए कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफतार करने की ठान ली थी किन्तु किसी तरह यह मामला टला। प्रदीप ने ही यह गीत भी लिखा था ‘जरा ऑंख में भर लो पानी’, जिसे सुनने के बाद पं.नेहरू की आँखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने पूछा था, इस गीत के रचयिता कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद नरेन्द्र शर्मा आए। वे भी साहित्य की मुख्य धारा के कवि थे। फिल्मों में उनके सैकड़ों गीत हिट हुए। साहित्यिक स्पर्श के गीत लिखने में भरत व्यास और शैलेन्द्र भी अग्रणी रहे, यद्यपि वे मुख्य् धारा के कवि न थे। गोपाल सिंह नेपाली भी जिस वक्त फिल्मों में गीत लिखने गए, कवि सम्मेालनों में उनकी तूती बोलती थी। तब तक चार-पाँच संग्रह उनके आ चुके थे। यद्यपि देशभक्ति और क्रांतिकारी गीतों का नेपाली का दौर फिल्मों से वापसी के बाद शुरू होता है। पर फिल्मों में उनके लिखे गीतों ने जनमानस में एक गहरी छाप छोड़ी। बोलचाल की लय में ढले उनके गीतों के बोलों को सुनकर एक फिल्म के सेट पर उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि मैं तो समझती थी कि उर्दू ही सबसे मीठी जुबान है लेकिन आज पता लगा कि हिन्दी से मीठी कोई जुबान नहीं है। उन्होंने सफर, शिकार, बेगम, लीला, गजरे, शिवभक्तव, तुलसीदास, शिवरात्र, जयश्री, राजकन्याी, सती मदालता, गौरीपूजा, नागपंचमी, नागकन्याब, माया बाजार, नरसी भगत, नई रोशनी, मजदूर, जय भवानी, आदि पचास से अधिक फिल्मों मे तीन सौ से ज्याादा गीत लिखे। किन्तु फिल्म जगत से कोई समझौता नहीं। किया फिल्मों में गीत लिखते हुए भी उनके आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छे न थे, विमल राजस्थानी के नाम लिखे पत्र से यह बात जाहिर भी होती है। आज इतनी तकनीकी तरक्की के बावजूद हमारे पास नेपाली के लिखे और उस समय के महत्वपूर्ण गायकों द्वारा गाए ज्यादातर गीतों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिनके बिना नेपाली के समग्र अवदान का मूल्यांकन कठिन है।
जीवन-संघर्ष
नेपाली ने थोड़ी ही वक्त में जीवन के विराट सत्य का साक्षात्कार किया था। फिल्मों में घाटा उठाने के बाद वे अपने शुद्ध कवि-जीवन में लौट आए थे। जिस तरह लोग जीवन के लिए नाना किस्म के समझौते करते हैं और सतही उद्देश्यों के लिए मनुष्यता के पतन की निम्नतर पायदान पर आ पहुँचते हैं, नेपाली ने ऐसा कुछ नही किया। वे तो कहते थे—‘तुझ-सा लहरों में बह लेता/ तो मैं भी सत्तात गह लेता/ईमान बेचता चलता तो/ मैं भी महलों में रह लेता/ हर दिल पर झुकती चली मगर, आंसू वाली नमकीन कलम/ मेरा धन है स्वाधीन कलम।‘––यह वही कविता है जिसे नेपाली जी जब मंचों पर सुनाते थे तो फिर उनके बाद किसी और कवि का मंच पर टिकना असंभव-सा हो जाता था। नेपाली ने छंदों के जादू को पहचान लिया था। इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली का अपना मिजाज बोलता है। एक लेखक कवि की स्वााधीन सत्ता और निजता क्या होती है, इसे नेपाली ने पहचाना और अपने जीवन में उतारा था। इसी स्वित्व् और स्वाभिमान के वशीभूत होकर उन्होंहने लिखा था—‘लिखता हूँ अपनी मर्जी से/ बचता हूँ कैंची दर्जी से/ आदत न रही कुछ लिखने की/ निंदा-वंदन खुदगर्जी से/ कोई छेड़े तो तन जाती, बन जाती है संगीन कलम/ मेरा धन है स्वाीधीन कलम।‘ पर इस स्वाधीन कलमकार की विडंबना देखिए। ऊपर से लगता है फिल्मों का इतना बड़ा गीतकार, जनता का पसंदीदा कवि जहाँ थोड़ी शोहरत मिलते ही मामूली से मामूली कवि भी अपने को ‘गीतों का राजकुमार’ कहलाना पसंद करते हों, नेपाली के जीवन के जद्दोजहद को बयान करता नेपाली पिक्चर्स के पैड पर 7 फरवरी, 1956 को विमल राजस्थानी के नाम लिखा उनका एक पत्र इंटरनेट पर मौजूद है। विमल ने शायद अपने पत्र में कुछ चुटकी ली होगी। पत्रोत्तसर के अंश देखिए—
“मूर्ख कहीं के। यहाँ सुरा–सुंदरी का फेर कहाँ है। जीवनयापन की कठोरता को रंगरेलियॉं नहीं कहना चाहिए। हॉं, कभी कभी टीस उठती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नही सका। सोचता हूँ शायद आगे कुछ कर सकें। अभी तो मैं ही भँवर में पड़ा हूँ। बेतिया के अपने घर वाले चैन से बैठने नही देते। बाप को रूपया भेजो, भाई को रूपया भेजो, अपना और परिवार की लन्तरानी अलग है। इन्हीं झंझटों में गीत भी लिखता हूँ, कविताऍ भी झाड़ देता हूँ। आमदनी मरीज के बुखार की तरह होती है। कभी कम कभी ज्यादा। अब बेतिया से खबर आई है कि एक जो टूटा-फूटा घर था, वह भी नीलाम हो रहा है या हो चुका है। भाई मुझे 15-20 दिन का समय चाहिए था अधिक से अधिक या तुम शिव बरन राय जो ग्रेन मर्चेंट है, छोटा रमना या बनारस बाबू से जरा इतनी बिनती नहीं कर दोगे। मै यथाशक्ति जल्द यानी इसी मास में बेतिया आ रहा हूँ। तब तक मेरा इंतजार करें। मैं आकर पैसे चुका दूँगा। यहॉ सांप्रदायिक बलवा के कारण पैसा थोड़ा रूका हुआ है। नही तो मैं इसी समय चल पड़ता। क्या दुनिया है? जिसने अपने गीतों और कविताओं से बेतिया और चंपारन के नाम की दुंदुभि सारे हिंदुस्तान में मचा दी, उसी महाकवि की झोपड़ी बेतिया वाले ही नीलाम कर रहे हैं। जय हो पैसा भगवान की।“
नेपाली ने इस संघर्ष की छाया अपनी रचनाओं पर नही पड़ने दी। वे उसी उमंग और उल्लास से गाते रहे: “मैं सरिता के कल-कल स्वर में अपना ही गायन सुनता हूँ।” या “उड़ उड़ कर गा रहे विहग जो /वह मेरा ही अमर गान है”
कविता: एक मिशन
नेपाली का कवि उमंग, पंछी और रागिनी में रोमानी कल्पनाओं से गुजरता हुआ, नीलिमा और पंचमी में प्रकृति के तत्वो से जीवन जीने की सरस प्रेरणा लेता है। बाद के एक दशक का दौर ऐसा भी है जहॉं नेपाली बम्बगई के फिल्मी जगत से जुड़ कर अपने गीतों को जन-जन की कसौटी पर आजमाते हैं परन्तु उन्होंने बालीवुड से जुड़ कर भी अपने गीतों का कद छोटा नहीं होने दिया, उसे अपनी साहित्यिक रचनाधर्मिता से सींचने का काम करते रहे। चित्रपट की मायानगरी में रह कर जहॉं अपने गीतों से उन्होंने खासा धनोपार्जन भी किया, अपनी फिल्में बनाने की धुन में गाढ़े की पूँजी गँवा बैठे। पर उनकी बौद्धिक पूँजी बदस्तूर उनके पास थी। यही वजह है कि जब वे फिल्मी दुनिया से लौट कर अपने घर यानी आम जनता के पास आए तो वे एक दूसरे ही नेपाली थे। यह वही दौर था जब आजादी के बाद का परिदृश्यप हमें लगातार सावधान करता था। गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा ही था, आज जीत की रात पहरुवे सावधान रहना। लिहाजा चीन के आक्रमण ने उनके कवि को जैसे एक मिशन दे दिया। ऐसे समय जब राष्ट्र कवि दिनकर की ओजस्वी वाणी क्षितिज में हुंकार कर रही थी, क्षितिज के एक ओर से दूसरे दिनकर यानी नेपाली जी का उदय हुआ। हिमालय ने पुकारा के अपने गीतों से बिना किसी राष्ट्रकवि का छत्र मुकुट धारण किए नेपाली ने चीन को बुरी तरह ललकारा और चालीस करोड़ देशवासियों को उठ खड़े होने का आह्वान किया। उनकी रचना “चलो भाई बोमडिला” सुनाते ही हजारों लोग एक साथ ताल देने लगते थे। वे मानते थे कि कवि कोई छोटा मोटा प्राणी नही है, वह चाहे तो इतिहास बदल सकता है। उनका विश्वास था:
“हर क्रांति कलम से शुरू हुई सम्पूर्ण हुईचट्टान जुल्म की, कलम चली तो चूर्ण हुईहम कलम चला कर त्रास बदलने वाले हैंहम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं”
इस मामले में वे अपने को वन मैन आर्मी कहा करते थे। वे राष्ट्रकवि के आसन पर भले न विराजमान रहे हों, लोगों के दिलों के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके थे। यही वह समय है जब वे चालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो, यह मेरा हिंदुस्ताान है, तुम कल्प़ना करो, नवीन कल्पनना करो, शासन चलता तलवार से, इतिहास बदलने वाले हैं, मुस्का्न पुरानी कहाँ गई तथा मेरा धन है स्वाधीन कलम जैसी ओजस्वी रचनाऍ मंचों पर सुना रहे थे। चालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा रचना कोई मामूली नही है। यह जागरण और आह्वान का गीत है। प्रयाण गीत है। कबीर कहा करते थे, दुखिया दास कबीर है जागै अरु रोवै। कुछ कुछ ऐसी पीर इस गीत में है कि सुनते ही धमनियों में लहू की गति तेज हो उठती थी: कुछ पदावलियॉ देखें—
“भूला है पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दोलम्पट है लुटेरा है तो ललकार के कह दोजो मुँह से कहा है वही तलवार से कह दोआए न कोई लूटने भारत को दुबारा।चालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा।
जागो कि बचाना है तुम्हें मानसरोवररख ले न कोई छीन के कैलाश मनोहरले ले न हमारी यह अमरनाथ धरोहरउजड़े न हिमालय तो अचल भाग्य तुम्हाराचालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा।”
कहते हैं इस गीत को सुनकर राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कवि को बधाई दी थी और कहा था कि इस कविता को हिंदी और उर्दू में छाप कर सारे भारत में बँटवा देना चाहिए। ऐसी ही एक उबलता हुआ गीत है, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो। सीमा समस्या पर इससे अच्छा गीत शायद ही कोई हो। आजादी तो हमने अहिंसा के बलबूते ली थी पर कहीं इसे हमारी कमजोरी न मान लिया जाए, नेपाली इस बात से वाकिफ थे। इसीलिए वे इस मामले में थोड़े हार्डलाइनर थे। शीश झुकाना और फरियाद करना उन्हें गवारा न था। है ताज हिमालय के सिर पर—गीत में वे लिखते हैं—
“अब दिल्ली वह दरबार नहीं, यह परवानों की महफिल हैहै नई शमा उम्मीउदों की, आजाद एशिया का दिल हैइस दिल की धड़कन में धड़के, लाखों अरमान करोड़ों केराजा हो एक, प्रजा लाखों, अब ऐसा यहाँ रिवाज नहींहै ताज हिमालय के सिर पर, अब और किसी का ताज नहीं।”
इन पंक्तियों से हमें नेपाली की वैचारिक बुनावट का अहसास होता है। वे नवीन कल्पना करने के लिए कहते हैं तो किसी निजी चित्तेवृत्ति के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए। कवि देश के लिए पहले सोचता था। निज गौरव नहीं, बल्कि देश-गौरव से ओत-प्रोत नेपाली ने ऐसा बहुत कुछ लिखा है–जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हर समय ऐसे मूल्यों, उद्बोधनों की प्रासंगिकता बनी रहेगी—
“हम थे अभी अभी गुलाम, यह न भूलनाकरना पड़ा हमें सलाम, यह न भूलनारोते फिर उमर तमाम, यह न भूलनाथा फूट का मिला इनाम, यह न भूलनाबीती गुलामियॉ न लौट आऍ फिर कभीतुम कल्पाना करो नवीन कल्प ना करो”
नेपाली जी ने दिल्ली सरकार को संबोधित एक रचना लिखी थी, ‘शासन चलता तलवार से।‘ शायद वे सरकार से तमाम मामलों में सख्त रुख की अपेक्षा रखते थे। याद हो तो दिनकर ने भी ऐसी एक रचना दिल्ली को संबोधित करके लिखी है: ‘भारत का यह रेशमी नगर’ शीर्षक से। कहना न होगा कि जीवन की अर्धशती आते आते नेपाली के भीतर का क्रांतिकारी कवि जाग उठा था । वह जानता था कि दिनकर की धरती को एक और नेपाली की प्रतीक्षा है। एक और कवि धरती को चाहिए जो राष्ट्र के बारे में, राष्ट्ररभाषा के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में और स्वाधीन कलम के बारे में खुल कर बोले। मानव की समता के बारे में बोले, देश को, समाज को जगाए। वे स्वराज ही नहीं, सुराज चाहते थे। एक गीत में उन्होंने लिखा है–
“स्वतंत्रता मिली हमें कि देश में ‘सुराज’ होमनुष्य एक आज हो कि वर्ग एक आज होसमाज के लिए समाज का अखंड राज होमनुष्ये मांगता यही, यही मनुष्य मानताकि हो समाज राज में मनुष्यर की समानता।”
इस तरह एक कवि का कर्तव्यों निबाहने में नेपाली सदैव अग्रणी रहे।
वे समता और समानता के कायल थे। उन्हें इस बात का रंज था कि हमारा घर तो घर के रखवालों ने लूटा है। इस भावना को उन्होने नौ लाख सितारों ने लूट में पिरोया है। उन्होंने इस विडंबना की ओर याद दिलाया कि जो जेल से लौट आए वे इनाम के हकदार बने, जो जेल न जा सके वे मात खा गए और जिनकी इहलीला जेल में ही समाप्त हो गयी, उन्हें सब भुला बैठे। उनका कहना था: ‘स्वप्न टूटते रहे, कल्पेना मरी नहीं/ रोटियॉ गरीब की प्रार्थना बनी रहीं।‘ कभी कभी उनके भीतर का क्षुब्ध मन दुखी भी होता था। उन्हों ने पंचमी के गीत—‘जग से हमसे दो दिन न बनी ‘ में लिखा है—
“अफसोस नही इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सकेझोलियॉ किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सकेअपने प्रति सच्चा रहने का, जीवन भर हमने यत्न कियादेखा-देखी हम जी न सके, देखा-देखी हम मर न सके।”
गीति काव्य : लिरिक की साधना
जिन अर्थों में गीत को लिरिक कह कर पुकारा जाता है, वह पश्चिम की देन है। हमारा प्राचीन काव्य छांदिक संरचना का महान उदाहरण है। जिस तरह ग्रीक लिरिककारों ने कविता में गीतितत्वों का विधान किया– चासर से लेकर शेक्स पियर तक के सानेट उससे प्रभावित हुए, जर्मन कवि गेटे में जिस गीतितत्वा की सघनता देखने को मिलती है, जिसका कीर्तिमान आगे चल कर वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स और ब्राउनिंग आदि के कृतित्व में मिलता है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में छायावादी काव्यधारा दशकों तक प्रवहमान रही, जिसका रम्यक रूप संस्कृात में कालिदास के नाटकों में गुँथा हुआ है, शाकुंतल के पन्ने जिस तरह के लिरिकल आवेग में फड़फड़ाते हैं, जिस लिरिक की संवेदना का वहन जयदेव और मैथिल कवि विद्यापति करते हैं बल्कि जयदेव की अभिनवता और लिरिक का आश्रय ग्रहण कर ही वे आगे चल कर अभिनव जयदेव कहलाए, उस लिरिक में नवता का आह्वान विद्यापति ने तेरहवी सदी में किया—नव वृन्दाएवन, नव-नव तरु-गन/ नव-नव विकसित फूल/ नवल बसन्ता नवल मलयानिल/मातल नव अलिकूल। ध्यान रहे कि बीसवीं सदी के महान हिंदी कवि निराला ने भी अपनी सरस्वती वंदना में नव का अनकेश: प्रयोग किया है। नव गति, नव लय, ताल-छंद नव/नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;/नव नभ के नव विहग-वृंद को/ नव पर, नव स्वर दे !
हिंदी में लिरिक के यशस्वी कवियों में निराला, पंत, महादेवी और प्रसाद हैं। निराला की गीतिका और अनामिका की रचनाएं, प्रसाद के आंसू, पन्त के पल्लव और गुंजन, महादेवी की नीरजा में गीति की –लिरिक की संवेदना सघन है। हिंदी की गीति-चेतना को रवीन्द्रवनाथ टैगोर ने भी काफी प्रभावित किया है। कुल मिलाकर यह जो लिरिक की धारा है वह हिंदी के आधुनिक बड़े कवियों से होती हुई दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा और तदुपरांत केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, शिवमंगल सिंह सुमन और गिरिजाकुमार माथुर तक प्रवहमान दिखती है।
युगीन प्रासंगिकता और नेपाली
सवाल यह है कि गोपाल सिंह नेपाली जिस गीत या गीति धारा का संवर्धन करते हैं, उसकी युगीन प्रासंगिकता क्या है। नेपाली ने अपने संग्रहों में अपनी कविताओं के बारे में बहुधा लिखा है। उससे यह पता चलता है कि बचपन में वे ब्रजभाषा की कोमलकांत पदावली से अभिभूत हुए तो उमर खय्याम की रुबाइयों से भी। उन्होंने अपने से सवाल किया था कि उसके गीतों में विचार हों, चिंताएँ हों या रोजमर्रा के खर्च की चीजों की फेहरिस्त हो। राग हो या रोटी। वे लिखते हैं:
“आधुनिक हिंदी काव्य वीणा में जो मेरा स्वच बज रहा है वह पता नहीं, आपके लिए रोमांच है, सिहरन है गुदगुदी है या शब्दों की दुलत्ती। हाँ, मैं एक कल्पना मजे में कर सकता हूँ और वह यह कि जाड़े की काली सनी डरावनी रात है। चारो ओर बर्फ पड़ रही है और उस अँधेरे में मेरा क्षीण स्वर जाड़े से ठिठुर कर आपके कानों के दरवाजें पर सर मार रहा है और आप है कि गरम गरम रजाई की तहों के भीतर नींद के मजे ले रहे हैं। जैसे ऊपर से तेल छिड़क कर दियासलाई लगा देने भर की देर हो।”
इसका अर्थ यह है कि वे अपनी कविताओं को अपनी कसौटी पर कसते रहते थे। उसकी प्रभावत्ताक और सार्थकता का आकलन करते रहते थे। और इसके लिए वे प्रकृति के पास जाते थे, उससे प्रेरणाएँ लेते थे। उनके यहाँ भोर, प्रभात, संध्या, तारों, मेघ, लहर, पंछी, वसंत, वन , पतझड़, प्राची, मेघ, सावन, नन्ही बूँदें, दोपहरी, अम्बर के चित्र हैं तो प्रिय-आगम और जीवन के राग को सींचने वाली काव्यात्मकक जिजीविषा भी। कहना न होगा कि कविवर रवीन्द्ररनाथ टैगोर पर लिखी रचना में उनके जिस विशेषत्वी का अनुगायन नेपाली ने किया है, उन विशेषताओं और काव्यरगुणों के प्रति कहीं न कहीं एक ललक नेपाली जी के कवि-मन में भी रही है।
“कालिदास तुम, तुम कबीर थेतुम तुलसी गंभीर धीर थेतुम गायक कविश्रेष्ठ सूर थेनयनों के दो बूँद नीर थे।”
यह समूची कविता इस बात का उदाहरण है कि वह कवि रवीन्द्ररनाथ ठाकुर के जीवन और कृतित्वल से कितना ओतप्रोत रहा है। वे कविता को बोलचाल की लय से जोड़ने वाले कवि थे। “तुम्हारी इतनी सच्ची बात, उड़ा दी हँसकर मैंने आज” —कितनी सहजता है इस पंक्ति में। जैसे यह पारस्परिक संवाद हो।
नेपाली को याद करते हुए जिन कुछ कविताओं को रेखांकित करना जरूरी है, उनमें ‘बाबुल तुम बगिया के तरुवर’ जैसी कविता भी है। एक सधे हुए रूपक से अपनी बात उठाते हुए वे स्त्री की नियति का लेखा जोखा रखते हैं। पंक्तियाँ ऐसी कि उनमें धँसें तो आंसू आ जाएँ। सोचिये ऐसी ही पीड़ा से गुजरते हुए निराला ने कभी ‘सरोज स्मृति’ जैसी मार्मिक रचना लिखी होगी। बेटियां पराया धन कही जाती हैं। उन्हें पाल-पोस कर योग्य वर-घर के सुपुर्द करना होता है। बेटियों के लिए आज के एक शायर ने लिखा है—घर में रह के भी गैरों की तरह होती हैं/ बेटियाँ धान के पौधों की तरह होती हैं—-‘बाबुल तुम बगिया के तरुवर’ कविता में बेटी पिता को संबोधित करती है। सदैव बेटी का हित चाहने वाले पिता को क्या मालूम कि सुहाग की पहनी हुई चुनरी उसकी हथकड़ी बनने वाली है, जिस ससुराल वह जा रही है वह कांटों की फुलवारी बन जाएगी। बेटी कहती है, पैदा होने पर माँ पिता का हृदय जल उठता है, यौवन खिला तो ननद भाभियाँ जल उठती हैं, इस तरह नारी हृदय के अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। कवि ने इस कविता में जैसे परकायाप्रवेश कर नारी के अंतर्मन की थाह ली है। लोकभाषा की सी आभा में रची यह कविता सुन कर आंखें बरस पड़ती हैं। इसी तरह ‘दूर जाकर न कोई बिसारा करे’ और ‘दिल चुराकर न हमको भुलाया करो’ जैसी मार्मिक और भावसंकुल रचनाऍं है जिन्हें कवि ने हृदय के गीले कोरों से रचा है।
नेपाली के जीवन की अर्धशती संघर्षों में ही बीती। अल्प शिक्षा, परिवार के आर्थिक संकट, फिल्मों में घाटा, घर की नीलामी, यशस्वी कवि होकर भी फाकेमस्ती और दूर तक कहीं न बुझने वाली प्यास ने नेपाली के कवि-मन को व्यथित ही नहीं किया, भलीभांति मथा भी था। पर उन्होंने निज के संकटों का रोना अपनी कविताओं में नहीं रोया। समाज और देश की व्यथा-कथा लिखने में ही उनका जीवन बीत गया। वे होते तो उनकी आगामी रचनाओं में कविता की, देश की, समाज की और भी बांकी छवि हमें देखने को मिलती। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपाली का रचना-संसार सदैव स्मृति में धारण करने योग्य है और रहेगा।।